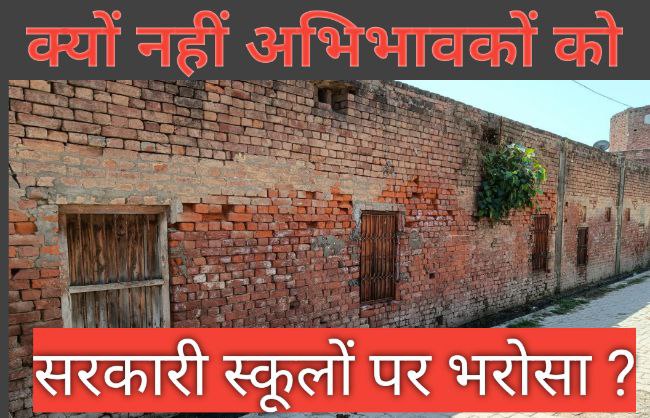हालिया अध्ययन ने पुष्टि की है कि शिक्षा की खराब गुणवत्ता के कारण माता-पिता को सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं है और वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाना पसंद करते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें ट्यूशन और अन्य फीस पर काफी अधिक खर्च करना पड़े। आज देश भर के सरकारी स्कूल गरीबों और अशिक्षितों के बच्चों का सहारा बन गए, जहां उन्हें नौकरशाही और शिक्षक संघों की दया पर रहना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप इन स्कूलों के लिए स्थापित मानकों-पाठ्यपुस्पुतकों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता, विद्यार्थियों की उपलब्धियों का निरीक्षण का विकास थम गया। आज नब्बे प्रतिशत से ज्यादा सार्वजर्वनिक खर्च की राशि भारतीय स्कूलों में अध्यापकों के वेतन और प्रशासन पर ही खर्च होती है। फिर भी विश्व में बिना अनुमति अवकाश लेने वाले अध्यापकों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। हमारे स्कूलों में अध्यापक आते ही नहीं हैं और चार में से एक सरकारी स्कूल में रोज कोई न कोई अध्यापक छुट्टी पर होता है।
आईआईएम अहमदाबाद के शिक्षा का अधिकार संसाधन केंद्र के एक हालिया अध्ययन ने पुष्टि की है कि शिक्षा की खराब गुणवत्ता के कारण माता-पिता को सरकारी स्कूलों पर भरोसा नहीं है और वे अपने बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला दिलाना पसंद करते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें ट्यूशन और अन्य फीस पर काफी अधिक खर्च करना पड़े। बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने के लिए परिवारों द्वारा बताये गए दो सबसे प्रमुख कारण है – सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता के प्रति असंतोष और पास में कोई सरकारी माध्यमिक विद्यालय का न होना। विद्यालय भी अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं या इसकी खराब गुणवत्ता से ग्रस्त हैं। हालांकि स्कूल भवन, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन खेल के मैदानों, कंप्यूटरों और रैंप के मामले में स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इस वजह से सरकारी स्कूल गरीबों और अशिक्षितों के बच्चों का सहारा बन गए, जहां उन्हें नौकरशाही और शिक्षक संघों की दया पर रहना पड़ता है।
इसके परिणामस्वरूप इन स्कूलों के लिए स्थापित मानकों-पाठ्यपुस्पुतकों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता, विद्यार्थियों की उपलब्धियों का निरीक्षण का विकास थम गया। आज नब्बे प्रतिशत से ज्यादा सार्वजर्वनिक खर्च की राशि भारतीय स्कूलों में अध्यापकों के वेतन और प्रशासन पर ही खर्च होती है। फिर भी विश्व में बिना अनुमति अवकाश लेने वाले अध्यापकों की संख्या भारत में सबसे अधिक है। हमारे स्कूलों में अध्यापक आते ही नहीं हैं और चार में से एक सरकारी स्कूल में रोज कोई न कोई अध्यापक छुट्टी पर होता है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2022 के अनुसार, बच्चों की सरल अंग्रेजी वाक्यों को पढ़ने की क्षमता कक्षा V के बच्चों के लिए 2016 के स्तर पर बनी हुई है (2016 में 24।7% से 2022 में 24।5% तक)। 2022 में 68।9% स्कूलों में खेल का मैदान है, लड़कियों के लिए उपयोग योग्य शौचालयों वाले स्कूलों में 2022 में केवल 68।4% की वृद्धि हुई है, पीने के पानी की उपलब्धता वाले स्कूलों का अनुपात सिर्फ 76% है।
यूनेस्को की 2021 की भारत के लिए शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार: कोई शिक्षक नहीं, कोई कक्षा नहीं, भारत में लगभग 1।1 लाख स्कूल एकल-शिक्षक संस्थाएँ हैं। 2022 में शिक्षकों की औसत उपस्थिति 87।1% है और पिछले कई वर्षों से औसत छात्र उपस्थिति लगभग 72% बनी हुई है। सुधार के बावजूद, कुछ क्षेत्रों में लिंग असमानताएँ बनी हुई हैं। नामांकित न होने वाली 15-16 साल की लड़कियों के अनुपात में गिरावट जारी है, जो 2022 में 7।9% हो गई है। भारत में प्राथमिक स्तर की कक्षा (1-5) में स्कूलों में ड्रॉपआउट की कुल दर 1।5 प्रतिशत है, उच्च प्राथमिक कक्षा (6-8) में 3 प्रतिशत है। माध्यमिक स्तर की कक्षा (9-10) में 12 प्रतिशत के साथ उच्चतम स्थान है जो अभी भी एक बड़ी चुनौती है। 2022 में किसी न किसी रूप में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा में नामांकित 3-वर्षीय बच्चों का अनुपात 78।3% है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ) को समय-समय पर संशोधित किया जाता है, लेकिन पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता को लेकर चिंताएं हैं।
उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 पारंपरिक पाठ्यक्रमों की तुलना में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों में कम नामांकन का संकेत देता है। कोविड-19 महामारी ने डिजिटल विभाजन को उजागर किया, जिसमें कई छात्रों के पास ऑनलाइन शिक्षा तक पहुंच नहीं थी। नीति आयोग 2023 के अनुसार, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों का स्कोर अधिक है, जबकि बिहार और झारखंड जैसे राज्यों का स्कोर कम है, जो शिक्षा की गुणवत्ता में असमानताओं को दर्शाता है। कक्षा I-VIII में सशुल्क निजी ट्यूशन कक्षाएं लेने वाले बच्चों का अनुपात 2018 में 26।4% से बढ़कर 2022 में 30।5% हो गया। ये सब बेहद चिंतनीय है। देश और राज्य सरकारों के लिए यह कम लज्जा की बात नहीं है कि जिन कामों को उन्हें खुद करना चाहिए, उनके लिए अदालतों को आदेश देना पड़ता है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा की बदहाली किसी से छिपी नही है। पूरे देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। कई स्कूलों में तो शिक्षक पढ़ाने ही नहीं जाते,जहां जाते हैं वहां वे मन से नहीं पढ़ाते।
इन स्कूलों की दशा सुधारने के लिए बना तंत्र भी लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। किसी का किसी पर नियंत्रण नहीं है। आज पूरे तंत्र पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सरकारी प्राथमिक स्कूलों की इस दशा को सुधारने के लिए सभी सरकारी अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और न्यायिक कार्य से जुड़े अधिकारियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे अपने बच्चे को पढ़ने के लिए इन्हीं स्कूलों में भेजें। सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों से अधिक आकर्षक बनाने की पहल की जा सकती है अगर पर्याप्त कक्षाएँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ और मनोरंजक सुविधाएँ सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाये। स्वच्छ पेयजल, क्रियाशील शौचालय और नियमित स्वच्छता जागरूकता अभियान, डिजिटल शिक्षण की सुविधा के लिए कंप्यूटर, टैबलेट और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच प्रदान की जाए। ओडिशा सरकार का 5टी हाई स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, टीम वर्क और परिवर्तन की ओर ले जाने वाली समयबद्धता की 5टी अवधारणा पर आधारित है।
2021 में लॉन्च किया गया यह कार्यक्रम सभी उच्च विद्यालयों में स्मार्ट और डिजिटल कक्षाओं, ई-पुस्तकालयों, आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाओं, बेहतर स्वच्छता सुविधाओं और खेल सुविधाओं के रूप में शैक्षिक प्रौद्योगिकी को अपनाने पर केंद्रित है। योग्यता-आधारित भर्ती लागू करना, प्रतिस्पर्धी वेतन प्रदान करना, और व्यावसायिक विकास के अवसर प्रदान करना,शैक्षणिक कौशल और विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए नियमित कार्यशालाएँ, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, शिक्षकों को प्रेरित करने और उनके प्रयासों को मान्यता देने के लिए प्रदर्शन-आधारित इनाम प्रणाली लागू करना इस दिशा में बेहतरीन प्रयास साबित हो सकता है। एक समग्र दृष्टिकोण को शामिल करना जो संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर केंद्रित हो। छात्रों को भविष्य में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करने के लिए व्यावसायिक कौशल और उद्यमशीलता प्रशिक्षण को एकीकृत करना,परियोजनाओं, क्षेत्र यात्राओं और व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करना, एक स्वागत योग्य और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना जो विविधता का सम्मान करता हो और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता हो।
विद्यार्थियों की प्रगति पर चर्चा करने और चिंताओं को दूर करने के लिए नियमित अभिभावक-शिक्षक बातचीत को प्रोत्साहित करना, स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की गतिविधियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों को शामिल करना जैसे ओडिशा सरकार का स्कूल अभियान, अपनी तरह की एक अनूठी पहल है जो ओडिशा में सरकारी स्कूलों के सुधार में योगदान करने के लिए पूर्व छात्र समुदाय को प्रेरित और संगठित करने का प्रयास करती है। ओडिशा के आदर्श विद्यालय (ओएवी) मॉडल का उद्देश्य सुलभ, गुणात्मक और सस्ती अंग्रेजी माध्यम शिक्षा प्रदान करके ग्रामीण शहरी अंतर को पाटना है। अब तक ओडिशा के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के सभी 314 ब्लॉकों में 315 अंग्रेजी माध्यम के सह-शिक्षा हैं। इन पहलों को लागू करके, हम एक अधिक न्यायसंगत और समावेशी शिक्षा प्रणाली बना सकते हैं, जो प्रत्येक बच्चे को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए सशक्त बनाती है। इसका उद्देश्य सशक्त, सुसज्जित और नैतिक युवाओं की एक पीढ़ी का निर्माण करना है, जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों।
देश में माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, और इसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करते हुए, केंद्र और राज्य सरकारों- दोनों की वार्षिक शिक्षा योजना में इसे प्राथमिकता देकर माध्यमिक शिक्षा पर अधिक नीतिगत ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। सस्ती माध्यमिक शिक्षा का प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने, शिक्षकों के प्रशिक्षण, पर्याप्त शिक्षण-अधिगम संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और एक जवाबदेह और पारदर्शी शासन-व्यस्था की संरचना बनाने के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर समान ध्यान दिया जाना चाहिए। इस दिशा में जब तक कठोर उपाय नहीं किए जाते, वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक स्तर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करना दुर्ग्राह्य ही लगता है।

-प्रियंका सौरभ
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,उब्बा भवन, आर्यनगर, हिसार

Author: Jarnail
Jarnail Singh 9138203233 editor.gajabharyananews@gmail.com